भोपाल। 16 अप्रैल, 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक व समयानुकूल निर्णय सुनाया, जो न केवल भाषाई अधिकारों को संरक्षित करता है बल्कि इस गहरी सच्चाई की पुनः पुष्टि करता है कि भारत की विविधता उसकी कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत है।
आज जब भारत की सांस्कृतिक विविधता को राजनीतिक ध्रुवीकरण और वोट बैंक की रणनीति का हथियार बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक सशक्त संवैधानिक अनुस्मारक बनकर सामने आया है। एक ऐसे दौर में जब भाषाएं और पहचान राजनीतिक गणित के उपकरण बनती जा रही हैं, यह फैसला केवल कानूनी नहीं बल्कि नैतिक, ऐतिहासिक और मानवीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
भाषा का धर्म नहीं होता
मंगलवार को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए कहा कि उर्दू एक भारतीय भाषा है, जिसकी जड़ें इसी मिट्टी में हैं, और इसका किसी एक धर्म से संबंध नहीं जोड़ा जा सकता। महाराष्ट्र के अकोला स्थित पातुर नगर परिषद कार्यालय के साइनबोर्ड पर उर्दू को बनाए रखते हुए, न्यायालय ने न केवल नागरिकों के भाषाई अधिकारों की रक्षा की, बल्कि उस भाषा की गरिमा भी बहाल की जिसे लंबे समय से हाशिए पर डाला गया था। यह फैसला एक स्मरण है कि भारत की भाषाई-सांस्कृतिक बहुलता हमारी राष्ट्रीय एकता की नींव है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला अकोला जिले की पातुर नगर परिषद से जुड़ा था, जहां पूर्व नगर पार्षद वर्षा ताई और संजय बांगड़े ने याचिका दाखिल कर साइनबोर्ड से उर्दू हटाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि महाराष्ट्र में केवल मराठी का प्रयोग होना चाहिए। नगर परिषद ने बताया कि उर्दू 1956 से उपयोग में है और स्थानीय जनता इसे अच्छी तरह समझती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मांग को खारिज किया और उच्च न्यायालय के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा।
“गंगा-जमुनी तहज़ीब” का सम्मान
अपने निर्णय में पीठ ने टिप्पणी की – “भाषा संस्कृति का हिस्सा है, धर्म का नहीं।” अदालत ने उर्दू को भारत की गंगा-जमुनी तहज़ीब का प्रतीक बताते हुए इसे मिश्रित सांस्कृतिक विरासत का एक शानदार उदाहरण कहा। यह स्वीकारोक्ति उस समन्वयवादी परंपरा का उत्सव है, जिसमें भाषाएं और संस्कृतियां आपस में घुलती-मिलती रही हैं।
औपनिवेशिक विभाजन की विरासत पर प्रहार
न्यायमूर्ति धूलिया ने स्पष्ट किया कि अंग्रेजों ने ही भाषाओं को धर्म के आधार पर विभाजित करने का काम किया। अदालत ने कहा, “यह अंग्रेज़ थे जिन्होंने हिंदी को हिंदुओं और उर्दू को मुसलमानों से जोड़ने की शुरूआत की। यह उनकी ‘फूट डालो और राज करो’ की नीति का हिस्सा था।” इस विभाजन ने जो सांस्कृतिक नुकसान पहुँचाया, यह फैसला उसी के खिलाफ एक गूंजता हुआ प्रतिवाद है।
उर्दू की उपेक्षा नहीं, उसका सम्मान करें
अदालत ने कहा कि उर्दू भारत की छठी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और इसकी उपेक्षा इतिहास के साथ अन्याय है। यह केवल पाकिस्तान की भाषा नहीं है—बल्कि भारत की सड़कों, अदालतों, फिल्मों और साहित्य की भाषा है। इसे एक धार्मिक पहचान तक सीमित करना गलत है।
भाषाई बहुसंख्यकवाद और राजनीतिक ध्रुवीकरण
आज जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में उर्दू के सार्वजनिक प्रयोग को लेकर नेताओं द्वारा विरोध जताया जाता है, यह फैसला हवा में ताजगी का झोंका है। यह हमें याद दिलाता है कि भाषाएं संप्रेषण का माध्यम हैं, न कि सांप्रदायिकता का हथियार।
संविधान और नेहरू की दृष्टि
अदालत ने पंडित नेहरू के उस विचार को याद किया जिसमें उन्होंने हिंदी और उर्दू के मेल से बनी ‘हिंदुस्तानी’ को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी। न्यायालय ने कहा, “अगर विभाजन नहीं हुआ होता, तो ‘हिंदुस्तानी’ हमारी राष्ट्रीय भाषा होती।”
न्यायमूर्ति की कविता में भाषा का दर्द
एक मार्मिक क्षण में, न्यायमूर्ति धूलिया ने एक उर्दू कविता उद्धृत की:
उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली,
क्यों मुझको बनाते हैं ताज्जुब का निशाना,
मैंने तो खुद को कभी मुसलमान नहीं माना,
अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली।
यह कविता उर्दू के उस दुख को अभिव्यक्त करती है, जिसे अपनी ही मिट्टी में पराया बना दिया गया।
फैसले की अंतिम पंक्तियाँ: पूरे भारत के लिए संदेश
अदालत ने कहा, “जब हम उर्दू की आलोचना करते हैं, तो हम हिंदी की भी आलोचना करते हैं—क्योंकि ये दोनों एक ही पेड़ की शाखाएं हैं।” यह एकता और साझी विरासत की भावना को पुनर्स्थापित करता है।
भाषाएं पुल हैं, दीवारें नहीं
यह फैसला केवल उर्दू की कानूनी जीत नहीं है—यह उस भारत की जीत है जो अपनी भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता को गले लगाता है। जैसा कि न्यायालय ने कहा—”हमें सभी भाषाओं से दोस्ती करनी चाहिए।” यही भारत की आत्मा है।








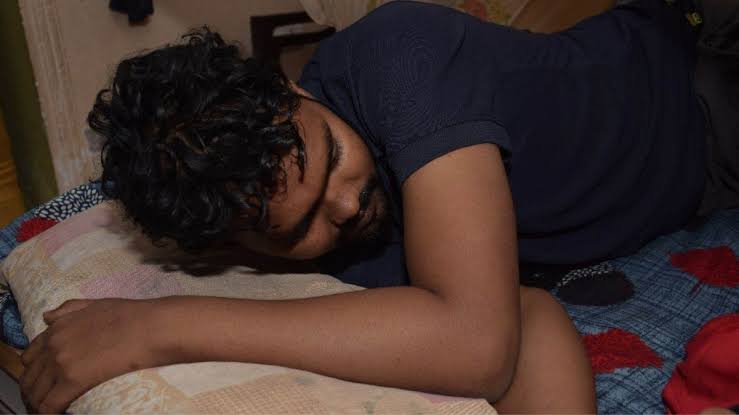





Leave a Reply